हिंदी व्याकरण से जुड़े Important Topic के प्रश्न एवं उन टॉपिक्स की विषयवार जानकारी दी हुई है। जिससे की आप को परीक्षा की तैयारियों में आसानी रहेगी एवं आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे। छात्र जो की SSC,IBPS, क्लर्क, बैंक आदि परीक्षाओं की तैयारियों कर रहे है वो सभी इस पेज से हिंदी के नोट्स (Hindi Grammar Notes in PDF) एवं महत्वपूर्ण प्रश्नो की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
Hindi Grammar Study Material in PDF
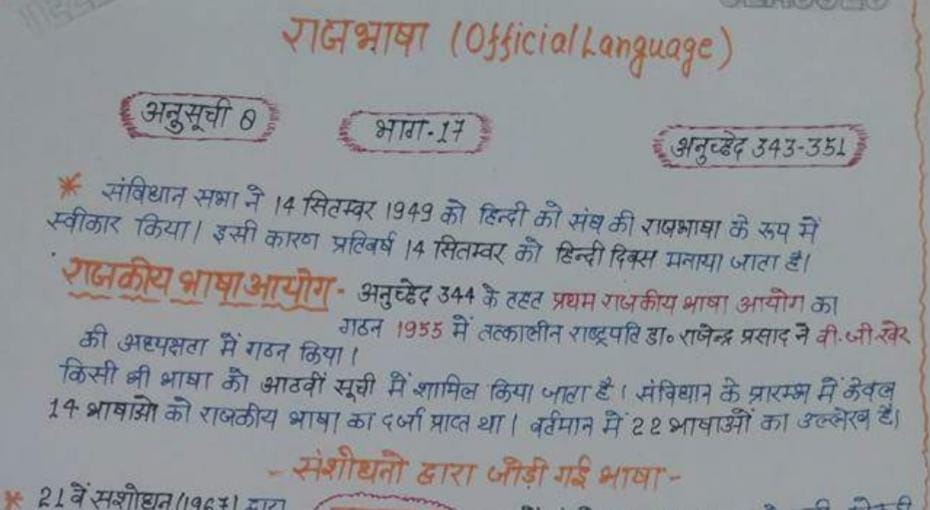
संज्ञा –
किसी व्यक्ति, वास्तु, नाम आदि के गुण धर्म, स्वाभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है जिनके नाम एवं उदहारण सहित जानकारी नीचे दी हुई है।
- व्यक्तिवाचक संज्ञा- संज्ञा जो की किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराये वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है।
- जातिवाचक संज्ञा- ऐसे शब्द जिनसे उसकी संपूर्ण जाती का बोध हो वह जाती वाचक संज्ञा कहलाती है।
- भाव वाचक संज्ञा- जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थो की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो वह भाव वाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण- आम में मिठास है।
- समुदायवाचक संज्ञा- जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति को वस्तुओं के समूह का बोध हो वह समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है।
- द्रव्य वाचक संज्ञा- जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु द्रव्य आदि पदार्थो का बोध हो वह द्रववाचक संज्ञा संज्ञा कहलाते है।
सर्वनाम-
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते है। यह 6 प्रकार के होते है।
- पुरुष वाचक सर्वनाम- पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते है।
- निश्चयवाचक सर्वनाम- किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते है।
- अनिश्चयवाचक सर्वनाम- ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते है।
- प्रश्नवाचक सर्वनाम- प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते है। उदाहरण- किसका, कौन, किसे आदि
- संबंध वाचक सर्वनाम- संबंध प्रकट करने वाले शब्द संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते है।
- निजवाचक सर्वनाम- ऐसे शब्द जिनसे करता के साथ अपनापन प्रकट होता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते है। उदाहरण- आप, अपना, मेरा आदि
- संयुक्त वाचक सर्वनाम- रूस के हिंदी व्याकरण के अनुसार कुछ पृथक श्रेणी के सर्वनामों को भी माना गया है जैसे की जो कोई, सब कोई, हर कोई आदि।
कारक-
वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यय या अप्रत्यय संबंध बना रहता है अथवा जो शब्द क्रिया सम्पादन में उपयोगी सिद्ध होते है उन्हें कारक कहते है। कारक 8 प्रकार के होते है।
कर्ता- ने
कर्म – को
करण – से , द्वारा
सम्प्रदान- के लिए
अपादान- से (अलग होने के लिए)
संबंध- का, के, की, रा, रे, री
अधिकरण- मे, पर
सम्बोधन- हे, औ, अरे
विशेषण एवं विशेष्य
- विशेषण – संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते है।
- विशेष्य- जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतायी जाये वह विशेष्य कहलाते है। उदहारण- गीता सुन्दर है इस वाक्य में सुन्दर विशेषण है एवं गीता विशेष्य है।
विशेषण 4 प्रकार के होते है-
- गुणवाचक विशेषण- जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते है।
- परिमाणवाचक विशेषण – जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्राय नापतोल का ज्ञान हो परिमाण वाचक विशेषण कहलाते है।
- संख्यावाचक विशेषण- जिन सह्ब्दों से किसी प्रकार की संख्या का बोध हो वे संख्या वाचक विशेषण कहलाते है।
- संकेतार्थक सर्वनाम वाचक विशेषण
समास
अनेक पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण करना समास कहलाता है । समास का अर्थ है संक्षिप्ति करण करना। यह 6 प्रकार के होते है।
- अव्ययीभाव समास- इनमे पहला पद अव्यय होता है एवं उस अव्यय पद का रूप, लिंग कारक वचन नहीं बदलता है।
समस्त पद – विग्रह
आजन्म – जन्म से
- तत्पुरुष समास – इसमें पहला पद गौण एवं बाद का पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का पद प्रधान होता है। इसमें बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तथा विग्रह करने पर करक चिन्ह प्रकट होता है।
- कर्म तत्पुरुष का उदहारण –
समस्त पद विग्रह
चिड़ी मार चिड़ी को मारने वाला
- कर्मधारय समास – जिन दो पदों के मध्य विशेषण- विशेष्य एवं उपनाम- उपमेय का भाव अन्तर्निहित होता है। तथा विग्रह करने पर सार रूप में प्रस्तुत हो जाता है। उदहारण-: नीलाम्बर – नीला है जो अम्बर
- द्वन्द्व समास – इसमें दोनों पद प्रधान होते है लेकिन उनके बीच में “या” अथवा और शब्द का लोप होता है | उदहारण -: राधा कृष्ण – राधा और कृष्ण
- द्विगु समास- पहला पद संख्यावाचक होता है एवं दूसरा पद प्रधान होता है। उदहारण- सप्ताह – सात दिनों का समूह
- बहुव्रीहि समास – इस समास में दोनों ही पद गौण होते है एवं उनमे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। उदहारण- घनश्याम – घन के सामान श्याम – विष्णु , त्रिनेत्र – तीन है जिनके नेत्र – शंकर
क्रिया –
जिस शब्द अथवा शब्द समूह जिसके अनुसार किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो क्रिया कहलाती है। उदहारण- अनु दूध पी रही है।
क्रिया के भेद – क्रिया 2 प्रकार की होती है।
- सकर्मक क्रिया – जिन क्रियाओ का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदहारण- लोग रामायण पढ़ते है।
- अकर्मक क्रिया- जिन क्रियाओ का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाते है। उदहारण-: गौरव रोता है
उपसर्ग – किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसको एक विशेष अर्थ प्रदान कर देना उपसर्ग कहलाता है।
उदहारण –
आ+ गमन – आगमन
प्र+ ताप – प्रताप
प्रत्यय –
किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश प्रत्यय कहलाते है।
उदहारण-
आवना- डरावना , लुभावना , सुहावना
ईन- प्राचीन, महीन
संधि एवं संधि विच्छेद
दो वर्णो से होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है।
- स्वर संधि- दो स्वरों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। यह ६ प्रकार की होती है।
- दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि एवं पररूप संधि
- व्यंजन संधि – एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों के योग से मिलने वाली ध्वनि का जो विकार पैदा होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है।
- विसर्ग संधि- यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तो उसके बाद आने वाले शब्द से स्वर अथवा व्यंजन के साथ योग होने से जो ध्वनि का विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है।
मुहावरे
विलक्षण एवं चमत्कार पूर्ण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते है।
अंग गिराना- उत्साह दिखाना
लोकोक्तियाँ/ कहावते
अर्थ को पूर्णतया स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य लोकोक्ति कहलाता है।
उदहारण- अपनी पगड़ी अपने हाथ – अपना सामान बचाना अपने हाथ में होता है।
शुद्ध- अशुद्ध वर्तनी
हिंदी में शब्द उच्चारण एवं लेखन की दृष्टि से शब्द शुद्धियो का ज्ञान आवश्यक है।
अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द
आविस्कार आविष्कार
ख़याल ख्याल
शुद्ध- अशुद्ध वाक्य
संरचना की दृष्टि से पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते है। भाषा में शब्दों के रूप, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अव्यय, काल, वचन आदि व्याकरणिक तत्व वाक्य की शुद्धता में सहायक होते है।
अशुद्ध वाक्य- मै तुम चलेंगे ।
शुद्ध वाक्य- मै और तुम चलेंगे।
विराम चिन्हो का प्रयोग-
अभियक्तियो की पूर्णता हेतु वक्त द्वारा बोलते समय शब्दों पर कहीं और जोर देना पड़ता है या कभी ठहरना पड़ता है और कभी कभी विशेष संकेतो का सहारा भी लेना पड़ता है।
- पूर्ण विराम (।) – महेश सो रहा है।
- अलप विराम (,) – प्रकाश ने सेब, आम और संतरा खाये
- अर्ध विराम (;) – जब तक हम गरीब है; बलहीन है, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता।
- प्रश्नवाचक चिन्ह (?)- आप कहाँ जा रहे है?
- विस्मयादिबोधक या सम्बोधन सूचक चिन्ह- (!) – अरे यह क्या हुआ ! हे भगवान उसकी रक्षा करो ।
- अवतरण चिन्ह- एकल उद्धरण चिन्ह (‘ ‘)- रामधारी सिंह ‘दिनकर’ प्रसिद्ध कवि है।
- दोहरा उद्धरण चिन्ह- (” “) – तिलक ने कहा “स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है”
- निर्देशक चिन्ह (-) – आँगन में ज्योत्स्ना-चांदनी छिटकी हुई थी।
- समास चिन्ह- माता- पिता, रण- भूमि
- कोष्ठक ( ), { }, [ ] – राम ने (हँसते हुए) कहा।
- विवरण चिन्ह (:) – क्रिया के २ भेद है :
- संक्षेप सूचक चिन्ह (.)- दिनांक – दि.
- लोप सूचक (…) (+++) – मै तो परिणाम भोग ही रहा हूँ कही आप भी…
- उपविराम (:) रश्मिधनू : एक समीक्षा
- तुल्यता सूचक चिन्ह- पवन= हवा
पर्यायवाची शब्द –
समान अर्थ वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है।
युवती – तरुणी , श्यामा, रमणी, सुंदरी
मूंगा- रक्तमणि, रक्तांग, प्रवाल
विलोम शब्द –
किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते है।
जैसे- सत्य-असत्य ,
ज्ञान – अज्ञान ,
नवीन -प्राचीन
क्रिया – प्रतिक्रिया
श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द –
ऐसे शब्द जो उच्चारण एवं लेखन में काफी समानता लिए हुए होते है लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता के कारण अलग अलग होते है।
अभिराम – सुन्दर
अविराम- लगातार
अध्- पाप
अध- आधा
तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्द
हिंदी भाषा में व्यत्पत्ति की दृष्टि से पांच प्रकार के शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं अर्धतत्सम
- तत्सम शब्द- वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते है।
- अर्धतत्सम शब्द- वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हो कर हिंदी में आये है।
- तद्भव शब्द- ऐसे संस्कृत के शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए है।
तत्सम – तद्भव
अंगरक्षक – अंगरखा
आशीष – आसीस
वाच्य–
वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह बोध होता है की कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है की वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है।
वाच्य के भेद –
- कृत वाच्य- जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, उसे कृत वाच्य कहते है। इसमें वाक्य का उदेश्श्य क्रिया कर्ता का कर्ता है। अर्थात क्रिया में कर्ता की प्रधानता है। उदहारण – सोहन पत्र लिखता है।
- कर्मवाच्य – इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उदहारण- पत्र लिखा जाता है।
- भाव वाच्य – इस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया भाव के अनुसार होती है। उदहारण- रमेश से बैठा नहीं जायेगा।
| Size | 17.6 MB |
| Pages | 70 |
| Subject | Grammer |
| Language | Hindi |
इस PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे Download Book लिखा होगा वहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है
Download Pdf
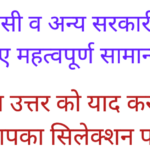




Leave a Reply